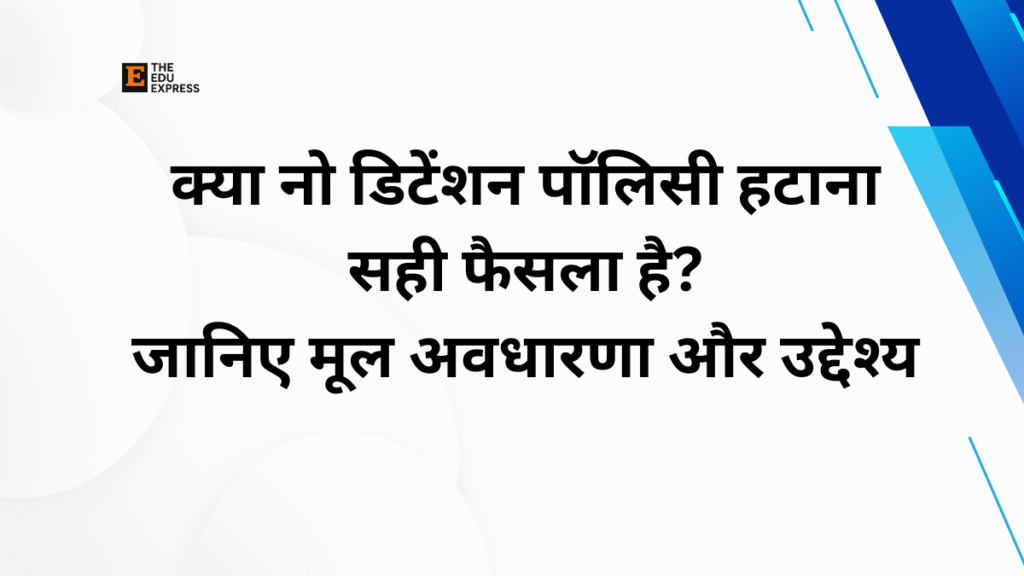नो डिटेंशन पॉलिसी (NDP) की जड़ें धारा-16, राइट टू एजुकेशन (RTE) अधिनियम 2009 में हैं, जिसके अनुसार “कक्षा 1 से 8 तक किसी भी बच्चे को रोका या निष्कासित नहीं किया जाएगा”। इस प्रावधान का मतलब यह था कि प्रत्येक विद्यार्थी को स्वचालित प्रमोशन मिलता रहे, भले ही वह वार्षिक परीक्षा में न्यूनतम अंक हासिल न कर पाए।
मुख्य उद्देश्य
- ड्रॉप-आउट कम करना – पिछली सदी के अंत में प्राथमिक स्तर पर ड्रॉप-आउट दर 40% से अधिक थी; लगातार प्रमोशन से यह दर 12.6% तक घट गई।
- तनाव-मुक्त सीखना – वार्षिक “पास-फेल” दबाव हटाने से छोटे बच्चों में परीक्षा का भय कम करना।
- समावेशिता – हाशिए के वर्गों, विशेषकर SC/ST, मुस्लिम व ग्रामीण छात्रों को स्कूल से जुड़े रखने के लिए संरक्षण देना।
मूलभूत तंत्र: CCE
RTE ने नो डिटेंशन पॉलिसी के साथ-साथ Continuous and Comprehensive Evaluation (CCE) लागू किया, जिसमें लिखित-मौखिक परीक्षण, प्रोजेक्ट, बातचीत इत्यादि से वर्षभर सीखने की प्रगति आँकी जाती है। नीति-निर्माता इसका अर्थ “बिना मूल्यांकन” नहीं, बल्कि “पारंपरिक वार्षिक परीक्षा के विकल्प में सतत व विविध मूल्यांकन” मानते हैं।
नो डिटेंशन पॉलिसी मुद्दा क्यों बना ?
नो डिटेंशन पॉलिसी को हटाने का निर्णय भारत के शिक्षा क्षेत्र में काफी चर्चा में है। यहाँ हम इस फैसले के पीछे के तथ्यों, आंकड़ों, संबंधित हितधारकों के तर्कों, और इससे जुड़ी प्रमुख चुनौतियों का विस्तार से विश्लेषण करेंगे। साथ ही, यह भी समझेंगे कि इस कदम का दीर्घकालिक प्रभाव क्या हो सकता है और क्या यह वास्तव में सही निर्णय था या नहीं।
फैसले का आधार: तथ्य और आंकड़े
पिछले दो वर्षों का डेटा कहता है कि भारत में कक्षा 5 और 8 में छात्रों का प्रतिशत पहले से ही गिर रहा है। NCERT के आंकड़ों के अनुसार, विज्ञान और गणित में छात्रों का पास प्रतिशत गिरकर 55% से 48% पहुंच गया है। विशेष रूप से पिछड़े इलाकों में इस गिरावट की दर अधिक है। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) के 2024 के रिपोर्ट के अनुसार, स्कूली शिक्षा में डिटेंशन रेट (छोड़ने की दर) हर साल लगभग 20% है।
इससे स्पष्ट होता है कि सरकार का निर्णय उन इलाकों में और अधिक dropout rates को रोकने के लिए है, जहाँ शिक्षा का अभाव अधिक है। डाटा यह भी दिखाता है कि अब तक लगभग 60% स्कूल बिना किसी प्रभावी अनुशासन नीति के काम कर रहे हैं। इससे सीखने का माहौल प्रभावित हो रहा है, और कई शिक्षकों का मानना है कि बिना डिटेंशन के समयबद्ध सुधार और अनुशासन बनाना संभव नहीं है।
इस निर्णय के तर्क और हितधारक
सरकार का तर्क है कि नो डिटेंशन नीति से छात्रों में नकारात्मक आत्ममूल्यांकन और असफलता का भय बढ़ रहा है। ये स्थिति छात्रों के आत्मविश्वास को नुकसान पहुंचाती है, और खराब परिणामों की चक्रवात बन जाती है।
शिक्षकों और स्कूल प्रबंधन का तर्क है कि बिना डिटेंशन के छात्रों को समर्थन और सुधार का अवसर कम हो रहा है। उनका कहना है कि अकादमिक प्रदर्शन में सुधार के लिए निरंतर निगरानी और अनुशासन आवश्यक है, जिससे पढ़ाई का स्तर ऊंचा रहे। अधिकारियों का मानना है कि इस कदम से dropout rates थमेंगे और अधिक छात्र स्कूलों में रहेंगे। लेकिन, साथ ही, यह भी सच है कि यदि सही तरीके से सुधार कार्यक्रम नहीं लागू किए गए, तो अनियमितता और पढ़ाई का स्तर गिरने का खतरा है।
मुख्य चुनौतियां और संभावित प्रभाव
डाटा कहता है कि बिना डिटेंशन के मामलों में, छात्र की अवधारणात्मक समझ और परीक्षा स्कोर दोनों प्रभावित हो सकते हैं। यदि सुधार कार्यक्रम प्रभावी नहीं रहे, तो यह नीति बड़े पैमाने पर सीखने की बाधा बन सकती है। एक और चिंता यह है कि यह निर्णय नई असमानताओं को जन्म दे सकता है। ग्रामीण और पिछड़े इलाकों में, जहां विशेष सहायता की आवश्यकता है, वहां शिक्षकों और प्रबंधन की अपर्याप्तता समस्या बढ़ सकती है। सामाजिक और मनोवैज्ञानिक प्रभाव के भी संकेत हैं। कुछ छात्र अपने प्रदर्शन को लेकर अधिक चिंतित हो सकते हैं, और परीक्षा से बाहर होने का डर बढ़ सकता है, जिससे आत्मसम्मान और मनोबल प्रभावित हो सकता है।
यह नीति सही है या नहीं: आंकड़ों की दृष्टि से
यदि हम आंकड़ों पर नजर डालें, तो यह स्पष्ट है कि डिटेंशन रेट को नियंत्रित करने के लिए समुचित समर्थन सिस्टम का अभाव है। इसलिए, सरकार का यह कदम, यदि साथ में मजबूत समर्थन और सुधार कार्यक्रम लागू किए जाएं, तो यह फायदेमंद हो सकता है। लेकिन, यदि इस नीति का क्रियान्वयन बिना तैयारी के किया गया, तो यह छात्रों के भविष्य के लिए नुकसानदायक हो सकता है। तटस्थ निष्कर्ष यही है कि, सही तरीका और सही समय पर इसे लागू करना जरूरी है।